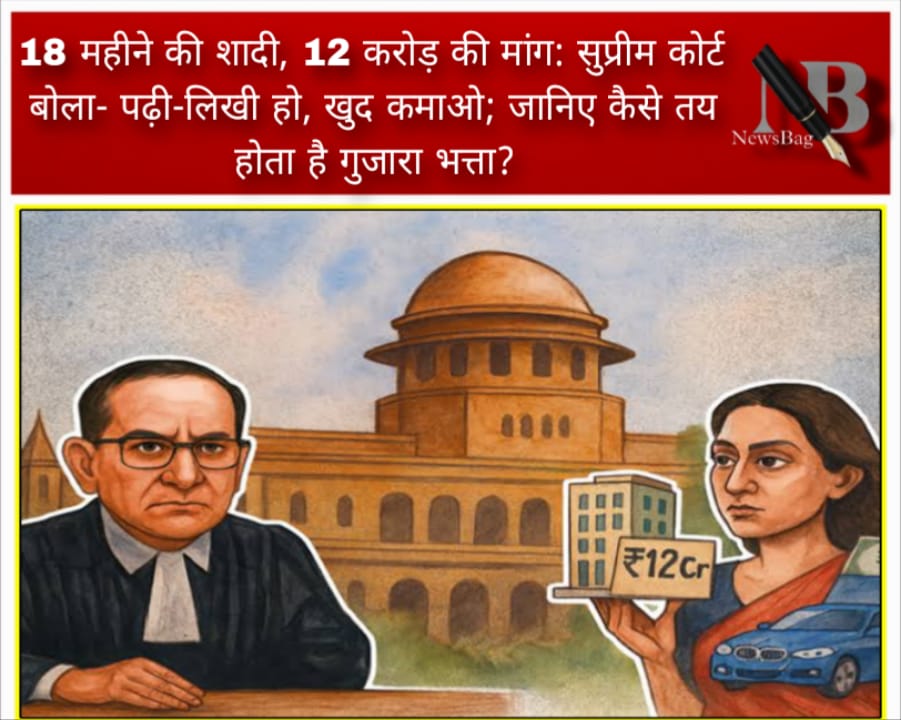
18 महीने की शादी, 12 करोड़ की मांग:

सुप्रीम कोर्ट बोला- पढ़ी-लिखी हो, खुद कमाओ; जानिए कैसे तय होता है गुजारा भत्ता?
दिल्ली | शादी को हुए थे सिर्फ 18 महीने, लेकिन पत्नी ने तलाक के बाद पति से जो मांग रखी, वह किसी को भी चौंका सकती है। एक एमबीए ग्रैजुएट महिला ने सुप्रीम कोर्ट में गुज़ारा भत्ते के तौर पर ₹12 करोड़, एक BMW कार और मुंबई जैसे मेट्रो शहर में लग्ज़री फ्लैट की मांग रख दी। लेकिन कोर्ट ने इन मांगों को असंगत मानते हुए महिला से कहा, “आप पढ़ी-लिखी हैं, काबिल हैं, फिर क्यों नहीं खुद कमातीं?”
यह मामला अब पूरे देश में बहस का विषय बना हुआ है—क्या कोई इतनी बड़ी राशि मांग सकता है? क्या कोर्ट सिर्फ महिला होने के कारण उसे बिना काम के भत्ता दे सकता है? और क्या पढ़ी-लिखी महिला से आत्मनिर्भर बनने की अपेक्षा अनुचित है?
मामला क्या है?
एक महिला, जो एमबीए की पढ़ाई कर चुकी है और आईटी सेक्टर में काम कर चुकी है, उसने अपने पति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। उसने मांग की कि उसे:
₹12 करोड़ की एकमुश्त राशि दी जाए,
एक BMW कार दी जाए,
मुंबई में एक लग्ज़री फ्लैट (जो पति के नाम है) उसे बगैर किसी कानूनी अड़चन के सौंप दिया जाए।
यह सब उस स्थिति में हुआ जब पति ने तलाक के लिए याचिका डाली और कोर्ट के सामने यह भी कहा कि पत्नी मानसिक रूप से अस्थिर (schizophrenic) है और उसने झूठे आरोप लगाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहा?
मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने जब इस मामले को सुना तो उन्होंने महिला की मांगों पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा:
कोर्ट ने तल्ख लहजे में महिला को समझाया कि अलिमनी (गुजारा भत्ता) का मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए करोड़ों की मांग करे क्योंकि उसने शादी की थी।
कोर्ट ने क्या सुझाव दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने महिला को दो विकल्प सुझाए:
1. वह पति की तरफ से ऑफर किए गए फ्लैट को कानूनी रूप से बिना शर्त स्वीकार कर ले।
2. या वह ₹4 करोड़ की एकमुश्त राशि लेकर समझौता कर ले।
महिला ने ₹12 करोड़ की मांग दोहराई, लेकिन कोर्ट ने उसे साफ शब्दों में कहा कि वह आत्मनिर्भर बनें और अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ें।
अलिमनी (गुजारा भत्ता) कैसे तय होता है?
भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के “राजनेश बनाम नेहा” (Rajnesh v. Neha) केस में अलिमनी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि गुज़ारा भत्ता तय करते वक्त इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:
1. शादी की अवधि – जितनी छोटी शादी, उतना कम भत्ता।
2. महिला की योग्यता और आय क्षमता – क्या महिला पढ़ी-लिखी है? क्या वह काम कर सकती है?
3. पति की कमाई और संपत्ति – क्या वह भत्ता देने की स्थिति में है?
4. पारिवारिक ज़िम्मेदारियां – बच्चों और माता-पिता की ज़िम्मेदारी किस पर है?
5. पूर्व में दिए गए भत्ते या उपहार – शादी में मिले गहने, घर, कार आदि को भी ध्यान में रखा जाता है।
6. पति-पत्नी का जीवन स्तर – शादी के दौरान कैसा जीवन रहा?
7. पत्नी की वर्तमान आय – अगर वह पहले से कमाती है, तो गुज़ारा भत्ता घटाया जा सकता है।
इन सभी पहलुओं को देखकर कोर्ट तय करता है कि भत्ता दिया जाए या नहीं और दिया जाए तो कितना।
आत्मनिर्भरता पर कोर्ट का जोर क्यों?
इस मामले में महिला एक पेशेवर थी, उसके पास एमबीए की डिग्री थी और वह आईटी सेक्टर में काम कर चुकी थी। कोर्ट का मानना था कि ऐसी स्थिति में उसे करोड़ों की मांग करने के बजाय नौकरी करनी चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए।
इस तरह की टिप्पणी देश में महिला सशक्तिकरण की वास्तविकता को भी उजागर करती है। सिर्फ महिला होना ही अलिमनी पाने का आधार नहीं हो सकता। अगर महिला सक्षम है, तो कोर्ट उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है।
सामाजिक संदेश क्या गया?
इस मामले से एक बड़ा सामाजिक संदेश भी गया—गुजारा भत्ता सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब ऐसे मामले जिनमें सक्षम महिलाएं भी करोड़ों की मांग करती हैं, उन्हें अदालत गंभीरता से नहीं देखेगी।
कोर्ट ने कहा कि विवाह को वित्तीय लेन-देन का साधन न बनाएं। विवाह एक सामाजिक संस्था है और जब वह टूटती है तो समाधान भी व्यावहारिक होना चाहिए, न कि असंवेदनशील या अत्यधिक मांगों से भरा हुआ।
यह केस उन हजारों महिलाओं और पुरुषों के लिए उदाहरण बन सकता है, जो तलाक के मामलों में व्यावहारिक और न्यायसंगत समाधान की तलाश में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह स्पष्ट कर दिया कि गुजारा भत्ता तभी देना उचित होता है, जब सामने वाला पक्ष वास्तव में आश्रित हो। पढ़ी-लिखी, योग्य और अनुभव वाली महिला से उम्मीद की जाती है कि वह अपने लिए आजीविका खुद कमाए।
यह फैसला न केवल कानून की व्याख्या करता है, बल्कि समाज को एक स्पष्ट संदेश देता है – “अधिकार के साथ कर्तव्य भी निभाना जरूरी है।”






